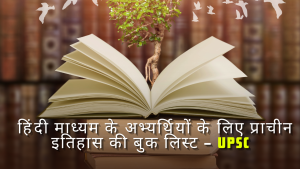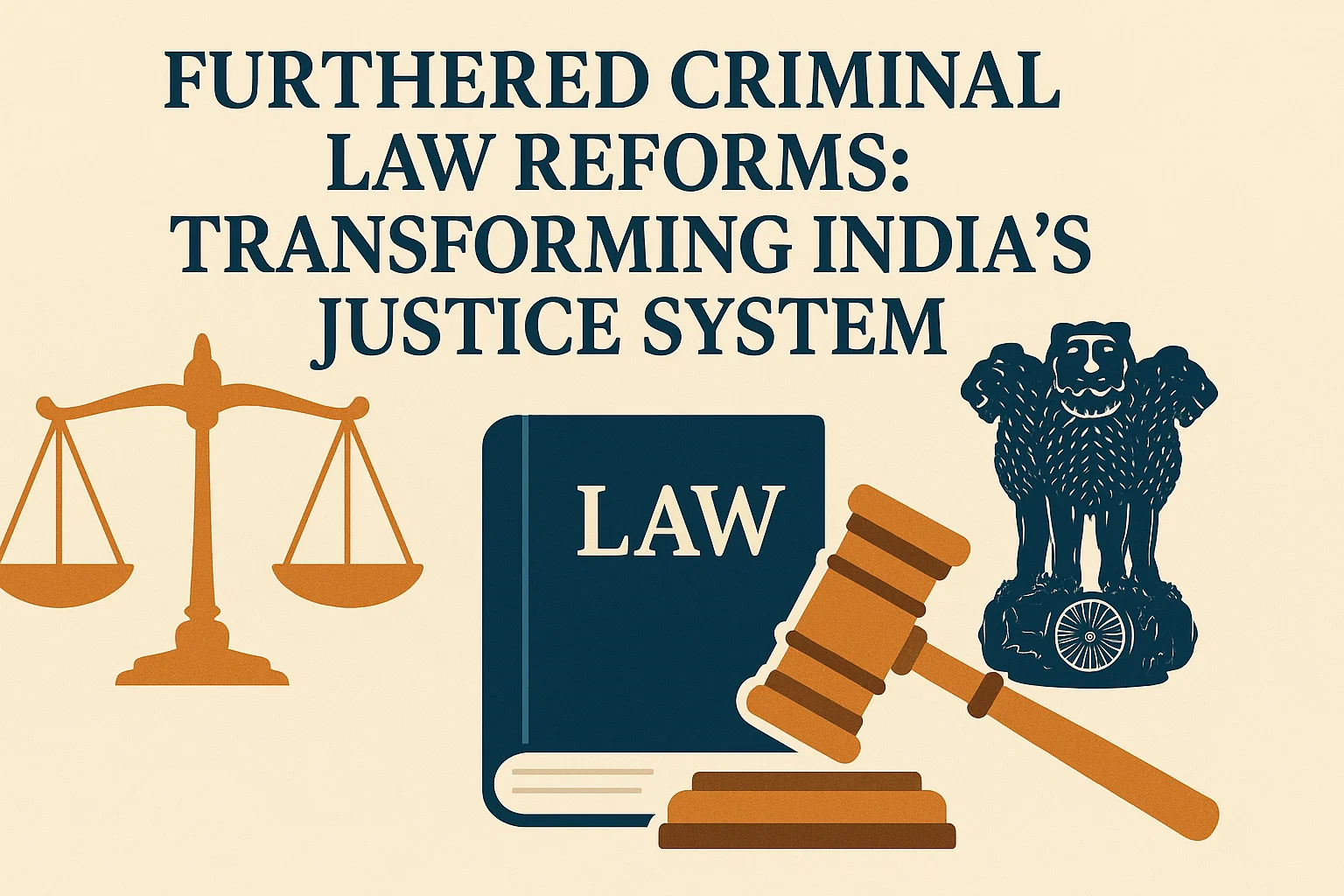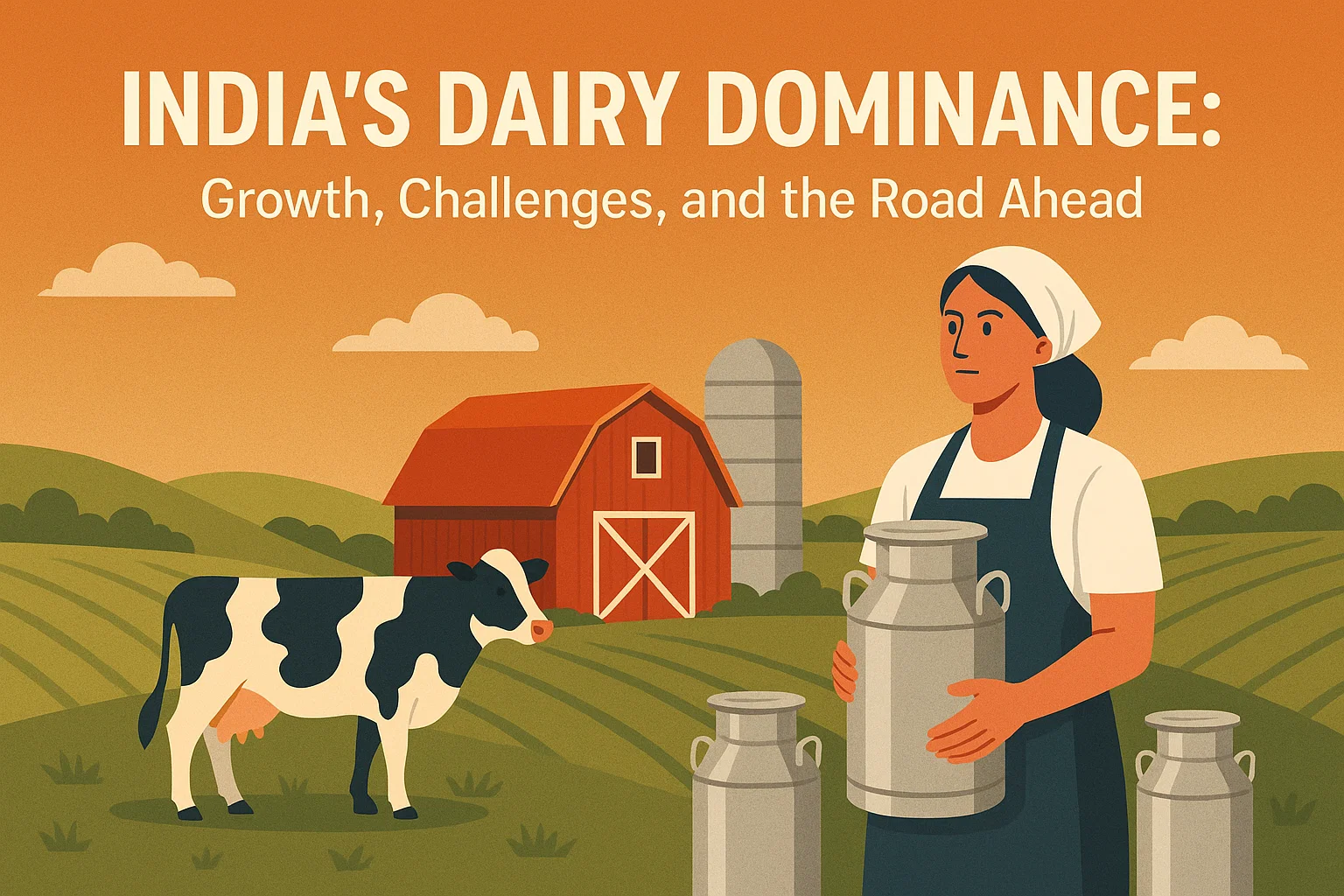दिल्ली सल्तनत: प्रारंभिक मध्ययुगीन परिवर्तन
दिल्ली सल्तनत (1206–1526) का UPSC केंद्रित विस्तृत सार — गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैय्यद, लोदी वंशों का इतिहास, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला व साहित्य।
दिल्ली सल्तनत (1206–1526)
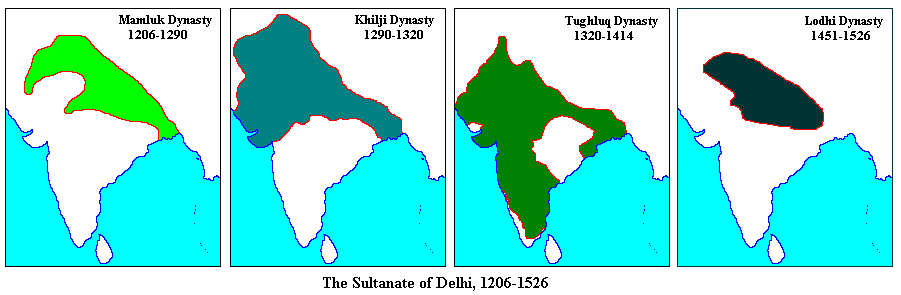
दिल्ली सल्तनत (1206–1526 ईस्वी) भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संक्रमणकाल था, जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन को संगठित और सुदृढ़ किया तथा आगे चलकर मुग़ल प्रशासन की ठोस नींव रखी। UPSC तैयारी के दृष्टिकोण से इसकी विशेष प्रासंगिकता इस तथ्य में है कि इसके राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान न केवल भारतीय मध्यकालीन इतिहास की दिशा तय करते हैं, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा (GS पेपर I) और मुख्य परीक्षा (GS पेपर I एवं इतिहास वैकल्पिक) में भी बार-बार पूछे जाते हैं।
गुलाम वंश (मामलुक वंश)
गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, का नाम अरबी शब्द ‘मामलुक‘ से लिया गया है। यह सैन्य भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित कुलीन तुर्की दासों को संदर्भित करता था, जो घरेलू या कारीगर दासों से अलग थे। इस काल में, तीन राजवंशों का उदय हुआ:
- कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित कुतुबी वंश (1206-1211 ई.),
- इल्तुतमिश द्वारा स्थापित प्रथम इल्बरी वंश (1211-1266 ई.),
- बलबन द्वारा नेतृत्व किया गया द्वितीय इल्बरी वंश (1266-1290 ई.)।
कुतुबुद्दीन ऐबक (1206–1210 ई.)
- यह मूल रूप से एक गुलाम था, इसने एक सैन्य कमांडर के रूप में मुहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त किया और बाद में 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद अपना शासन स्थापित किया।
- लाहौर से शासन किया और अपनी उदारता के लिए इसे लाख बख्श (“लाखों का दाता”) की उपाधि प्राप्त हुई।
- विद्वान हसन निज़ामी को संरक्षण दिया और कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की।
- चौगान (पोलो) खेलते समय एक दुर्घटना में मृत्यु। उसके पुत्र अराम बख्श को गद्दी मिली, पर शीघ्र ही इल्तुतमिश ने हटा दिया।
इल्तुतमिश (1211–1236 ई.)
- यह ऐबक का दास था और इल्बरी कबीले से संबंधित था । ऐबक की बेटी से विवाह कर गद्दी हासिल की।
- राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की।
- चंगेज खान और मंगोलों के साथ संघर्ष से बचने के लिए जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया।
- बंगाल, बिहार, सिंध और मुल्तान पर कब्ज़ा करके और राजपूत विद्रोहों को कुचलकर साम्राज्य का विस्तार किया।
- खलीफा से मंसूर (आधिकारिक मान्यता) प्राप्त करने वाले पहले सुल्तान, जिसने उसके शासन को वैध बनाया।
- रजत टंका (प्रारंभिक रुपया) जारी किया और चालीसा (चालीस अमीरों का दल) की स्थापना की।
- अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया।
रज़िया सुल्तान (1236–1240 ई.)
- दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक।
- एक अबीसीनियाई दास, याकूत, को उच्च पद पर नियुक्त करने और पर्दा प्रथा को अस्वीकार करने के कारण उसे विरोध का सामना करना पड़ा।
- अमीरों द्वारा अपदस्थ, बाद में भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया, लेकिन शीघ्र ही मारी गईं।
- उसकी मृत्यु के बाद चालीसा अमीरों का प्रभुत्व और बढ़ गया।
ग़ियासुद्दीन बलबन (1246–1287 ई.)
- सुल्तान बनने से पहले वह रिजेंट (नायब) के रूप में कार्य किया।
- निरंकुश राजतंत्र के समर्थक; स्वयं को “ज़िल्ल-ए-इलाही” (ईश्वर की छाया) कहा।
- प्रमुख सुधार:
- दरबार में कठोर अनुशासन (सिजदा, पैबोस प्रथा)।
- फ़ारसी पर्व नौरोज़ को शाही वैभव के प्रदर्शन हेतु शुरू किया।
- अमीरों पर नज़र रखने के लिए एक जासूसी तंत्र स्थापित किया।
- चालीसा को समाप्त किया, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और कानून-व्यवस्था बहाल की।
- सैन्य उपलब्धियाँ:
- दीवान-ए-अर्ज (सैन्य विभाग) की स्थापना।
- मेवाती डाकुओं को वश में किया और बंगाल विद्रोह को दबाया (विद्रोही तुगरिल खान को दबा दिया)।
- उसकी मृत्यु के बाद, उसके कमजोर पोते कैकुबाद को 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने उखाड़ फेंका, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया।
खिलजी वंश (1290-1320 ई.)
1290 से 1320 ई. तक, खिलजी वंश भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रभुत्व के चरम पर था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित, यह राजवंश अलाउद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी शासनकाल के लिए जाना जाता है, जिसने व्यापक प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक सुधार लागू किए।
जलालुद्दीन खिलजी (1290–1296 ई.)
- 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, साथ ही वह उदारता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था।
- मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद अपने महत्वाकांक्षी दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कारा का राज्यपाल नियुक्त किया। हालाँकि, 1296 में, अलाउद्दीन ने उसे धोखा दिया और गद्दी पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या कर दी।
अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316) – सत्ता का निर्माता
1. सत्ता का सुदृढ़ीकरण
- प्रारंभ में अमीरों को पुरस्कृत किया, परंतु बाद में कठोर नीतियों से विरोध को कुचल दिया।
- अमीरों पर नियंत्रण हेतु चार प्रमुख आदेश:
- विद्रोह रोकने हेतु संपत्ति की जब्ती।
- निगरानी के लिए गुप्तचर तंत्र का पुनर्गठन।
- दरबार में शराब और नशे पर प्रतिबंध।
- सामाजिक समारोहों के लिए शाही अनुमति आवश्यक।
2. सैन्य सुधार
- एक विशाल स्थायी सेना (475,000 घुड़सवार) बनाए रखी।
- इसके लिए पद्धति लागू किए:
- दाग़ – घोड़ों पर निशान लगाकर धोखाधड़ी रोकना।
- हुलिया – सैनिकों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना।
- नियमित निरीक्षण से अनुशासन सुनिश्चित करना।
3. बाज़ार सुधार (मूल्य नियंत्रण प्रणाली)
- सैनिकों को नकद भुगतान, जिससे मूल्य विनियमन आवश्यक हो गया।
- दिल्ली में चार प्रमुख बाज़ार स्थापित किए:
- अनाज
- कपड़ा, चीनी, फल, घी, तेल
- घोड़े, दास, पशु
- विविध वस्तुएँ
- प्रमुख अधिकारी:
- शहना-ए-मंडी (बाज़ार नियंत्रक)।
- नायब-ए-रियासत (व्यापार विभाग का प्रमुख)।
- मुन्हियान (उल्लंघन की सूचना देने वाले गुप्त एजेंट)।
- धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड के साथ सख्त मूल्य नियंत्रण।
4. भूमि राजस्व सुधार
- कर निर्धारण हेतु भूमि की माप करने वाला पहला सुल्तान।
- नकद (वस्तु के रूप में नहीं) में राजस्व एकत्र किया।
- शक्तिशाली जमींदारों पर भी कर लगाया, जिससे उनका प्रभाव कम हुआ।
- शेरशाह सूरी और अकबर के भावी सुधारों की नींव डाली।
सैन्य अभियान
1. मंगोल आक्रमण से रक्षा
- छह मंगोल आक्रमणों का सामना कर सभी को विफल किया।
- उत्तर-पश्चिम सीमा को मज़बूत किया।
- गाजी मलिक (बाद में गयासुद्दीन तुगलक) को मार्चेस का संरक्षक नियुक्त किया।
2. भारत में विस्तार
- गुजरात (1299) – विजय; रानी को बंदी बनाया गया; मलिक काफूर (भविष्य के सेनापति) को दिल्ली लाया।
- रणथंभौर (1301) – राजपूतों ने जौहर (सामूहिक आत्मदाह) किया।
- चित्तौड़ (1303) – प्रसिद्ध घेराबंदी; रानी पद्मिनी का जौहर (बाद में पद्मावत में रोमांटिक रूप दिया गया)।
3. दक्षिण भारत एवं दक्कन (मलिक काफूर के नेतृत्व में)
- देवगिरि (1307–08) – यादव राजा रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया।
- वारंगल (1309) – काकतीय राजा प्रतापरुद्र पराजित।
- द्वारसमुद्र (1310) – होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय ने आत्मसमर्पण किया।
- मदुरै (1311) – पांड्य राजा वीर पांड्य भागा; अपार धन-दौलत लूटी गई।
सांस्कृतिक योगदान
- अमीर खुसरो (कवि-संगीतकार) और अमीर हसन (सूफी कवि) को संरक्षण दिया।
- निर्माण कार्य:
- अलाइ दरवाज़ा (कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार)
- सीरी किला (दिल्ली का दूसरा नगर)
वंश का पतन एवं अंत
- 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी:
- मुबारक शाह (पुत्र, हत्या)
- खुसरो शाह (हड़पने वाला शासक, अलोकप्रिय)
- 1320 में, गाज़ी मलिक (दीपलपुर का गवर्नर) ने ख़ुसरो शाह की हत्या कर दी और गयासुद्दीन तुगलक के रूप में तुगलक वंश की स्थापना की।
तुगलक वंश (1320-1414 ई.)
ग़ियासुद्दीन तुग़लक़ (संस्थापक, 1320–1325)
- 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की।
- अपने पुत्र जौना ख़ाँ (बाद में मुहम्मद बिन तुगलक) के माध्यम से वारंगल के प्रतापरुद्र को पराजित किया।
- दिल्ली के निकट सुदृढ़ नगर तुग़लक़ाबाद का निर्माण कराया।
- 1325 में कथित रूप से अपने पुत्र जौना ख़ाँ द्वारा हत्या कर दी गई।
मुहम्मद बिन तुग़लक़ (1325–1351)
- महत्वाकांक्षी लेकिन विनाशकारी नीतियों के लिए प्रसिद्ध।
- साहित्य, धर्म और दर्शन का गहन ज्ञान।
- मिस्र, चीन और ईरान से राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- इतिहासकार बरनी, इसामी और इब्नबतूता ने उन्हें विरोधाभासी और जटिल शासक के रूप में वर्णित किया।
प्रमुख नीतियाँ व प्रयोग
राजधानी का स्थानांतरण (1327)
- दक्कन पर प्रशासनिक पकड़ मज़बूत करने के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी (दौलताबाद) स्थानांतरित की गई।
- जबरन पलायन से जनता को भारी कष्ट और मौतें हुईं।
- बाद में अव्यावहारिकता के कारण राजधानी पुनः दिल्ली लाई गई।
सांकेतिक मुद्रा (1329-30)
- चाँदी के स्थान पर ताँबे के सिक्के प्रचलन में लाए।
- व्यापक जालसाजी के कारण आर्थिक अराजकता फैल गई।
- योजना वापस लेनी पड़ी और जनता को चाँदी में भुगतान करना पड़ा, जिससे ख़ज़ाना खाली हो गया।
दोआब में कराधान में वृद्धि
- अकाल के दौरान कर बढ़ाए गए, जिससे किसान विद्रोह भड़क उठे।
- क्रूर उपायों से विद्रोहों को कुचला गया।
कृषि सुधार
- तकावी ऋण (कृषि अनुदान) की व्यवस्था।
- दीवान-ए-कोही (कृषि विभाग) की स्थापना।
- 70 लाख टंका खर्च करके एक आदर्श फार्म (64 वर्ग मील) की स्थापना की गई।
विद्रोह और पतन
- कई विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया:
- मदुरै सल्तनत (हसन शाह)
- विजयनगर साम्राज्य (1336)
- बहमनी साम्राज्य (1347)
- अवध, मुल्तान, सिंध, गुजरात (ताघी) में विद्रोह।
- 1351 में उनकी मृत्यु के बाद, सल्तनत कमज़ोर होने लगी।
- बदायूँनी की टिप्पणी: अंततः “सुल्तान प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा सुल्तान से।”
फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ (1351–1388)
- मुहम्मद बिन तुग़लक़ की मृत्यु के बाद अमीरों द्वारा चुना गया।
- खान-ए-जहाँ मकबल (एक धर्मांतरित तेलुगु ब्राह्मण) को अपना वज़ीर नियुक्त किया।
नीतियाँ और अभियान
- दक्कन पर पुनः विजय प्राप्त करने के बजाय उत्तर भारत को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- बंगाल पर असफल आक्रमण → बंगाल को स्वतंत्रता मिली।
- ओडिशा (जाजनगर) और नागरकोट में सफलता (कर वसूला गया)।
- ज्वालामुखी मंदिर से 1,300 संस्कृत पांडुलिपियाँ एकत्रित कीं → फारसी में अनुवादित।
- थट्टा (सिंध) में एक विद्रोह का दमन किया।
फ़िरोज़ शाह के प्रशासनिक सुधार
फिरोज तुगलक ने क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता दी। उसके शासन पर उलेमाओं (इस्लामी विद्वानों) का गहरा प्रभाव था, तथा उसने कई प्रमुख सुधार लागू किए:
-
- इक्ता प्रणाली का पुनरुद्धार: भू-राजस्व आवंटन को वंशानुगत बनाया।
- इस्लामी कर व्यवस्था:
- गैर-मुसलमानों पर जजिया कर सख्ती से लागू किया।
- सिंचाई कर (दिल्ली सल्तनत में पहली बार) लागू किया।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:
- नहरों का निर्माण किया, जिसमें सतलुज से हाँसी तक 200 किलोमीटर लंबी नहर और यमुना और हिसार को जोड़ने वाली एक अन्य नहर शामिल है।
- राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली के पास 1,200 फलों के बाग़ विकसित किए।
- आर्थिक व कल्याणकारी उपाय:
-
- 28 वस्तुओं पर अवैध करों को समाप्त किया।
- हज़ारों दासों को रोज़गार देने वाले कारखाने (शाही कार्यशालाएँ) स्थापित किए।
- फिरोज़ाबाद (फ़िरोज़ शाह कोटला) सहित 300 नए नगरों की स्थापना की।
- जामा मस्जिद और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं की मरम्मत की।
- दीवान-ए-ख़ैरात (अनाथों/विधवाओं के लिए कल्याण विभाग) की स्थापना की।
- सांस्कृतिक संरक्षण: बरनी और अफ़ीफ़ जैसे विद्वानों का समर्थन किया।
- धार्मिक असहिष्णुता:
- शियाओं, सूफ़ियों और हिंदुओं पर अत्याचार किए।
- गैर-मुसलमानों को दोयम दर्जे का दर्जा देने के लिए जजिया कर का इस्तेमाल किया।
- ग़ुलामों की संख्या को 180,000 दासों तक बढ़ा दिया, जिससे भविष्य में अस्थिरता पैदा हुई।
- उसकी मृत्यु (1388) के बाद, साम्राज्य कमज़ोर हो गया।
तैमूर का आक्रमण (1398)
- दिल्ली को तीन दिन तक लूटा और नरसंहार किया।
- 1399 में तैमूर की वापसी के बाद तुग़लक़ वंश का पतन तेज़ हो गया।
सैय्यद वंश (1414–1451)
- खिज़्र ख़ाँ (1414–21): तैमूर द्वारा मुल्तान का गवर्नर नियुक्त, उसने दिल्ली पर कब्जा किया और सैय्यद वंश की स्थापना की, लेकिन सुल्तान के रूप में नहीं, बल्कि रैयत-ए-आला के रूप में शासन किया। सिक्के तथा खुतबे तैमूर और बाद में शाहरुख के नाम पर थे।
- मुबारक शाह (1421–33): खिज्र खाँ के पुत्र, ने सल्तनत को मजबूत करने का प्रयास किया।
- मुहम्मद शाह (1434–43): लगातार षड्यंत्रों का सामना किया, सरदारों पर नियंत्रण खो दिया।
- आलम शाह (1443-51): कमज़ोर शासक; वज़ीर हामिद खाँ द्वारा बहलोल लोदी को आमंत्रित करने के बाद गद्दी छोड़ दी।
लोदी वंश (1451–1526)
पहला अफगान वंश (पूर्व शासक तुर्क थे)।
- बहलोल लोदी (1451-89): अफ़ग़ान मूल; लोदी वंश की स्थापना की। अफ़ग़ान सरदारों को समान मानकर समर्थन प्राप्त किया। जौनपुर, कालपी, धौलपुर पर कब्ज़ा किया; बहलोल ताँबे के सिक्के जारी किए।
- सिकंदर लोदी (1489-1517): महानतम लोधी शासक; बिहार, बंगाल और ग्वालियर तक साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासन में सुधार किया, सड़कें बनवाईं, न्याय सुनिश्चित किया। आगरा की स्थापना की (1504) और गैर-मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगाया।
- इब्राहिम लोदी (1517-26): अभिमानी और कठोर। सरदारों को अपमानित किया; विद्रोहों का सामना किया। पानीपत के प्रथम युद्ध (1526) में बाबर द्वारा पराजित और मारा गया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया।
दिल्ली सल्तनत की सामान्य विशेषताएँ
1. प्रशासनिक व्यवस्था
- एक मजबूत और सक्षम प्रशासनिक ढाँचे का विकास किया।
- इसका प्रभाव पतन के बाद भी जारी रहा और आगे के प्रांतीय राज्यों तथा मुग़ल प्रशासन को प्रभावित किया।
2. इस्लामी राज्य संरचना
- सुल्तान ख़लीफ़ा के प्रतिनिधि होने का दावा करते थे।
- ख़ुतबा (शुक्रवार का उपदेश) और सिक्कों पर ख़लीफ़ा का नाम अंकित होता था।
- बलबन ने ख़ुद को “ईश्वर की छाया” कहा, लेकिन फिर भी ख़लीफ़ा को मान्यता दी।
- इल्तुतमिश, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने ख़लीफ़ा से मंसूर (औपचारिक मान्यता) प्राप्त की।
सुल्तान की भूमिका
- सैन्य, कानूनी और राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार।
- कोई निश्चित उत्तराधिकार कानून नहीं—अक्सर सैन्य शक्ति द्वारा गद्दी हथिया ली जाती थी।
- अमीरों और उलेमा का उत्तराधिकार निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी।
- उदाहरण: इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी नामित किया, परंतु अमीरों की स्वीकृति आवश्यक थी।
केंद्रीय प्रशासन
मुख्य विभाग एवं अधिकारी
| विभाग / अधिकारी | कार्य |
| नायब | उप-सुल्तान; सामान्य प्रशासन की देखरेख। |
| वज़ीर | वित्त विभाग (दीवाने-विजारत) का प्रमुख। |
| आरिज़-ए-मुमालिक | सैन्य विभाग (दीवाने-आरिज़) का प्रमुख; भर्ती का कार्य, परंतु सेनापति नहीं। |
| सुल्तान | सर्वोच्च सैन्य सेनापति। |
| दीवाने-रिसालत | धार्मिक कार्य; मुख्य सदर द्वारा संचालित; मस्जिदों और मदरसों के लिए अनुदान प्रबंधन। |
| दीवाने-इंशा | शासक और अधिकारियों के बीच पत्राचार का प्रबंधन। |
सैन्य सुधार
- बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की।
- अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित रूप में इसे और मजबूत किया :
- 3 लाख सैनिको की विशाल सेना,
- घोड़ों पर दाग़ लगाने की प्रणाली (दाग़ प्रणाली),
- सैनिकों को नक़द वेतन देने की व्यवस्था।
न्याय व्यवस्था
- मुख्य क़ाज़ी न्यायपालिका का प्रमुख, प्रांतों में भी क़ाज़ी नियुक्त।
- मुसलमानों के लिए शरीयत कानून लागू; हिंदुओं के लिए ग्राम पंचायत व्यवस्था।
- आपराधिक क़ानून सुल्तान के नियमों पर आधारित।
स्थानीय प्रशासन
प्रांतीय संरचना
- प्रांतों (इक्ता) में विभाजित, मुक्ती या वली (कानून-व्यवस्था और राजस्व के लिए उत्तरदायी) द्वारा शासित।
प्रशासनिक प्रभाग
इक्ता (प्रांत) → शिक (ज़िले) → परगना (उप-ज़िले) → गाँव
प्रमुख स्थानीय अधिकारी
| अधिकारी | कार्य |
| शिकदार | शिक (ज़िले) का प्रमुख। |
| आमिल | परगना (गाँवों के समूह) का प्रमुख। |
| मुक़द्दम / चौधरी | गाँव का प्रधान। |
| पटवारी | गाँव का लेखाकार। |
दिल्ली सल्तनत के दौरान अर्थव्यवस्था
भू-राजस्व व्यवस्था
भूमि का वर्गीकरण
- इक़्ता भूमि — अमीरों/अधिकारियों को प्रशासनिक या सैन्य सेवाओं के बदले प्रदान की जाती थी।
- ख़ालिसा भूमि — सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में; इसका राजस्व शाही दरबार के लिए उपयोग होता था।
- इनाम भूमि — धार्मिक नेताओं/संस्थानों को कर-मुक्त अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती थी।
राजस्व संग्रह
- किसान अपनी उपज का एक-तिहाई से आधा हिस्सा कर के रूप में देते थे।
- अतिरिक्त करों से किसानों की स्थिति और खराब हो गई।
- बार-बार पड़ने वाले अकालों ने कठिनाइयों को और बढ़ा दिया।
कृषि सुधार
- मुहम्मद बिन तुगलक़ और फ़िरोज़ तुगलक़ ने प्रमुख सुधार किए :
- सिंचाई सुविधाएँ और तक़ावी ऋण (कृषि ऋण) प्रदान किए।
- जौ की जगह गेहूँ की खेती को बढ़ावा दिया।
- बागवानी को प्रोत्साहित किया (फिरोज तुगलक ने 1,200 फलों के बाग विकसित किए)।
- दीवान-ए-कोही – मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग।
शहरीकरण एवं व्यापार
नगरों का विकास
मुख्य नगर : दिल्ली (पूरब का सबसे बड़ा शहर), लाहौर, मुल्तान, ब्रौच, अन्हिलवाड़ा, लखनौती, दौलताबाद और जौनपुर।
व्यापार एवं वाणिज्य
- विदेशी व्यापार
- निर्यात : फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को निर्यात।
-
- मुल्तानी और अफ़ग़ान मुस्लिम व्यापारियों का प्रभुत्व।
- तर्देशीय व्यापार: गुजराती मारवाड़ियों और बोहरा मुसलमानों द्वारा नियंत्रित।
उद्योग एवं शिल्प
- वस्त्र: कपास और रेशम उद्योग फल-फूल रहे थे (रेशम उत्पादन शुरू हुआ)।
-
- कागज़ उद्योग का विस्तार हुआ (14वीं-15वीं शताब्दी)।
- अन्य शिल्प: चमड़ा उद्योग, धातु उद्योग और कालीन बुनाई (अधिक मांग)।
- शाही कारखाने: सुल्तान और कुलीन वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुएँ तैयार करते थे।
मुद्रा प्रणाली
| शासक | योगदान |
| इल्तुतमिश | चाँदी का टंका प्रचलित किया। |
| खिलजी काल | 1 चाँदी का टंका = 48 जिटल। |
| तुगलक़ काल | 1 चाँदी का टंका = 50 जिटल। |
| अलाउद्दीन खिलजी | दक्षिण भारतीय विजयों के बाद स्वर्ण दीनार जारी किए। |
| मुहम्मद बिन तुगलक़ | –टोकन मुद्रा की शुरुआत।
–8 केंद्रों से 25 प्रकार के स्वर्ण सिक्के ढाले। |
सल्तनतकालीन सामाजिक जीवन
हिंदू समाज
- जाति व्यवस्था: कठोर रही; ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था।
- महिलाओं की स्थिति:
- अधीन भूमिका, सती प्रथा।
- पर्दा प्रथा उच्च वर्ग की हिंदू महिलाओं (मुस्लिम प्रभाव) द्वारा अपनाई गई थी।
मुस्लिम समाज
- जातीय विभाजन: तुर्क, अफ़गान, ईरानी, भारतीय मुसलमान – अंतरजातीय विवाह नहीं।
- धर्मांतरित हिन्दू: धर्मांतरण के बावजूद भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- कुलीन वर्ग: मुस्लिम अभिजात वर्ग प्रशासन पर हावी था, हिंदुओं द्वारा शायद ही कभी नियुक्तियाँ की जाती थीं।
जजिया कर
- गैर-मुसलमानों (ज़िम्मियों) पर “सुरक्षा कर” के रूप में लगाया जाता था।
- प्रारंभ में यह भू-राजस्व का हिस्सा था; फिरोज तुगलक ने इसे एक अलग कर बना दिया।
- ब्राह्मणों को कभी-कभी इससे छूट दी जाती है।
दिल्ली सल्तनत: कला, स्थापत्य, संगीत एवं साहित्य
स्थापत्य:
दिल्ली सल्तनत ने फ़ारसी एवं भारतीय शैलियों के संगम से इंडो-इस्लामिक स्थापत्य की शुरुआत की।
प्रमुख विशेषताएँ
- मेहराब, गुंबद, मीनारें और अरबी सुलेख प्रमुख हो गए।
- रंगीन संगमरमर, लाल/पीले बलुआ पत्थर पर भारतीय पत्थर-नक्काशी तकनीकों का उपयोग किया गया।
संरचनाओं का विकास
- प्रारंभिक चरण (मंदिर रूपांतरण)
-
-
- कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद (कुतुब मीनार के पास) — ध्वस्त हिंदू/जैन मंदिरों की सामग्री से निर्मित।
-
- मौलिक निर्माण
-
-
- कुतुब मीनार क़ुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण; सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित।
- अलाई दरवाजा (अलाउद्दीन खिलजी द्वारा)—अपने वैज्ञानिक गुंबद निर्माण के लिए उल्लेखनीय।
-
- तुगलक़ स्थापत्य
-
-
- धूसर पत्थर, मेहराब और गुंबदों का उपयोग।
- तुगलकाबाद किला (गयासुद्दीन तुगलक द्वारा) – इसमें एक कृत्रिम झील शामिल थी।
- गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और फिरोज शाह कोटला (फिरोज तुगलक द्वारा)।
-
- लोदी काल
-
- लोदी गार्डन (दिल्ली) — सल्तनत स्थापत्य के उत्तरकालीन स्वरूप को प्रदर्शित करता है।
संगीत
नवाचार एवं योगदान
- नए वाद्ययंत्र: सारंगी और रबाब का प्रचलन।
- अमीर खुसरो का योगदान:
- नए रागों (घोरा, सनम) की रचना।
- कव्वाली (फारसी और भारतीय संगीत का मिश्रण) का विकास।
- फारसी अनुवाद:
-
- फ़िरोज़ तुगलक़ के काल में रागदर्पण (भारतीय शास्त्रीय संगीत ग्रंथ) का अनुवाद।
- प्रमुख व्यक्तित्व:
- पीर भोधन (सूफी संत-संगीतकार)।
- ग्वालियर के राजा मान सिंह – संगीत को संरक्षण दिया; मान कौतूहल का संकलन किया।
साहित्य
भाषा एवं संरक्षण
- फ़ारसी को राजकीय दरबारी भाषा का दर्जा मिला।
- सुल्तानों के संरक्षण में अरबी और फ़ारसी साहित्य का विकास।
इतिहासकार एवं लेखक
| विद्वान | कृतियाँ |
| हसन निज़ामी | ताज-उल-मासिर |
| मिन्हाज-उस-सिराज | तबक़ात-ए-नासिरी |
| ज़ियाउद्दीन बरनी | तारीख-ए-फ़िरोज़शाही |
| शम्स-सिराज अफीफ | फ़िरोज़ तुगलक़ के शासन का विस्तृत विवरण |
अमीर ख़ुसरो (उस युग के महानतम फारसी कवि)
- सबक-ए-हिंद — भारतीय शैली में फ़ारसी कविता का विकास।
- ख़ज़ाइन-उल-फुतूह — अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विवरण।
- तुगलक़नामा — तुगलक़ वंश के उदय का वर्णन।
अनुवाद एवं क्षेत्रीय साहित्य
- ज़िया नक्शबी — संस्कृत से फ़ारसी में पहला अनुवाद (तूतीनामा)।
- राजतरंगिणी (कल्हण द्वारा) — कश्मीर के ज़ैनुल आबेदीन के काल में पुनर्जीवित।
- किताब-उल-हिन्द (अलबरूनी) — भारत पर प्रसिद्ध अरबी ग्रंथ।
क्षेत्रीय भाषाओं का विकास
- बंगाली — महाभारत का अनुवाद (नुसरत शाह द्वारा)।
- हिंदी — चंदबरदाई की कविताएँ।
- गुजराती और मराठी — भक्ति आंदोलन के कारण उन्नति।
- तेलुगु और कन्नड़ — विजयनगर शासकों के संरक्षण में विकास।
Subscribe to our Youtube Channel for more Valuable Content – TheStudyias
Download the App to Subscribe to our Courses – Thestudyias
The Source’s Authority and Ownership of the Article is Claimed By THE STUDY IAS BY MANIKANT SINGH